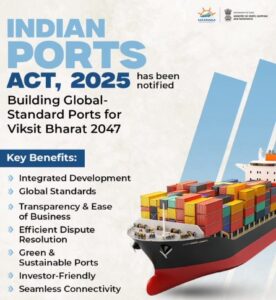खूंटी , 3 सितम्बर । झारखंड का खूंटी जिला प्राकृतिक संपदा से भरपूर इलाकों में गिना जाता है। घने जंगल, पहाड़ियां, नदियां और वन्यजीव यहां की पहचान रहे हैं। लेकिन इन्हीं जंगलों से जुड़े हाथियों का आतंक बीते पचास वर्षों से स्थानीय लोगों की जिंदगी को दहला रहा है। कभी खेतों को रौंदते हुए, कभी घरों की दीवारें तोड़ते हुए, तो कभी मासूम लोगों को रौंदते हुए गजराजों ने यहां के ग्रामीणों को भय और असुरक्षा का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है।
पिछले पांच दशकों में हाथियों के हमले से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों घर टूट चुके हैं और अनगिनत किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल हाथियों का आतंक नहीं, बल्कि एक गहरे असंतुलन की कहानी है, जिसमें इंसान और प्रकृति आमने-सामने खड़े हैं।

आंदोलन और अधूरी योजनाएं
हाथियों के इस आतंक से निजात पाने के लिए खूंटी और आसपास के जिलों के लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं। सड़क जाम, सरकारी कार्यालयों का घेराव, रेल रोको—हर तरह के प्रयास किए गए। स्थानीय संगठनों ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक गुहार लगाई कि कोई स्थायी समाधान निकले।
सरकार ने भी वादे किए। लगभग दो दशक पहले कर्रा प्रखंड के इंद्रवन (इंद वन) में हाथियों के लिए एक विशेष आश्रयणी बनाने की घोषणा की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया कि जिन इलाकों में हाथियों का हमला अधिक होता है, वहां बाड़बंदी कराई जाएगी और पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये योजनाएं कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाईं।
आज हालत यह है कि ग्रामीण कहते हैं—“सरकारी योजना सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित है, हमारे गांव तक नहीं।”
डर के साये में गांव
खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के गांव—डेरांग, रोन्हे, कालेट, गिड़ुम और एरमेरे—इन गांवों का नाम आते ही वहां के लोगों की पीड़ा सामने आ जाती है। कई ग्रामीणों ने तो खेती करना ही छोड़ दिया है।

किसान बताते हैं कि फसलें तैयार होते ही हाथी झुंड के झुंड खेतों में घुस जाते हैं और कुछ ही घंटों में महीनों की मेहनत को बर्बाद कर डालते हैं। घरों में रखा अनाज भी सुरक्षित नहीं रहता। महिलाएं अक्सर कहती हैं कि उन्हें रातभर जागकर पहरा देना पड़ता है। “सोने जाइए तो डर, जागिए तो डर। हाथी कब आ धमकेंगे, कहा नहीं जा सकता।”
वन विभाग की सीमित भूमिका
ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग का काम अब केवल औपचारिकता निभाने तक रह गया है। अगर हाथियों के हमले में किसी की मौत हो जाती है तो विभाग शव का पोस्टमार्टम कराता है और पीड़ित परिवार को कुछ हजार रुपये का मुआवजा देकर फाइल बंद कर देता है।
लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह पर्याप्त है? क्या सिर्फ मुआवजा देकर समस्या हल हो जाएगी? ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, खेती के लिए भरोसा चाहिए और जीने के लिए शांति चाहिए।
क्यों बढ़ रहा है संघर्ष?
झारखंड, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। आखिर क्यों?
रनिया प्रखंड के निवासी और सेवानिवृत्त वन प्रमंडल पदाधिकारी अर्जुन बड़ाईक बताते हैं कि असली वजह जंगलों की अंधाधुंध कटाई है। अवैध लकड़ी माफियाओं और खनन गतिविधियों ने हाथियों का आशियाना उजाड़ दिया है। जहां कभी घने जंगल और जलस्रोत हुआ करते थे, वहां अब सड़कें, कारखाने और बंजर जमीन बची है।
भोजन और पानी की तलाश में मजबूर हाथी जब गांवों की ओर आते हैं तो उनका सामना इंसानों से होता है। भूख और गुस्से में वे खेत, घर और कभी-कभी लोगों तक को कुचल देते हैं।

नक्सलवाद का असर
झारखंड में नक्सलियों की गतिविधियां भी इस संघर्ष को बढ़ा रही हैं। घने जंगलों में नक्सली कैंप और लगातार चल रही पुलिस-नक्सली मुठभेड़ों से हाथियों का प्राकृतिक आवास और असुरक्षित हो गया है। गोलीबारी और विस्फोटों से डरे हाथी झुंड छोड़कर भागते हैं और बस्तियों में घुस जाते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जंगल शांति का क्षेत्र न रहे तो वहां वन्यजीवों का रहना असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि हाथी अब इंसानी बस्तियों में भी दिनदहाड़े पहुंचने लगे हैं।
पीड़ितों की आवाज
खूंटी के एक किसान रामू महतो बताते हैं—“पिछले तीन साल से मैंने धान की खेती बंद कर दी। जितनी मेहनत करता था, उतनी बार हाथी सब बर्बाद कर जाते थे। अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ता है।”
इसी तरह एरमेरे गांव की एक महिला कहती हैं—“रात को बच्चों को लेकर डर से बाहर निकल जाती हूं। कभी खेत के किनारे, कभी पड़ोस के गांव में। अपने ही घर में अब चैन से नहीं सो सकते।”
ये आवाजें केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं हैं, बल्कि पूरे इलाके की सामूहिक वेदना हैं।
समाधान की तलाश
इस समस्या से निपटने के लिए केवल मुआवजा देना काफी नहीं है। विशेषज्ञ कुछ ठोस उपाय सुझाते हैं—
जंगलों की सुरक्षा – अंधाधुंध कटाई रोकनी होगी और खोए हुए जंगलों को फिर से बसाना होगा।
हाथी कॉरिडोर का निर्माण – हाथियों के पारंपरिक मार्गों को चिन्हित कर सुरक्षित बनाना जरूरी है ताकि वे बस्तियों में न घुसें।
सामुदायिक भागीदारी – ग्रामीणों को हाथी प्रबंधन की योजनाओं में शामिल करना होगा। उन्हें प्रशिक्षित कर गांव-स्तर पर सुरक्षा समितियां बनानी होंगी।
तकनीकी मदद – सोलर फेंसिंग, अलार्म सिस्टम और निगरानी ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर हाथियों को बस्तियों से दूर रखा जा सकता है।
त्वरित और पर्याप्त मुआवजा – पीड़ित परिवारों को पारदर्शी और समय पर आर्थिक सहायता मिले, ताकि वे खुद को असुरक्षित न महसूस करें।
हाथियों के आतंक की समस्या केवल स्थानीय नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए सबक है। अगर इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जारी रखेगा, जंगलों को काटेगा और वन्यजीवों के घर उजाड़ेगा तो टकराव होना ही है।
आज जरूरत है संतुलन बनाने की—इंसान और हाथी दोनों के लिए सुरक्षित स्थान तय करने की। तभी खूंटी जैसे इलाके चैन की नींद सो पाएंगे। वरना यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा और “गजराज का दंश” हर रोज़ नई पीड़ा लेकर सामने आता रहेगा।